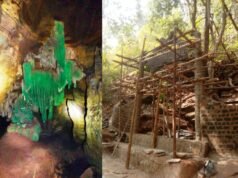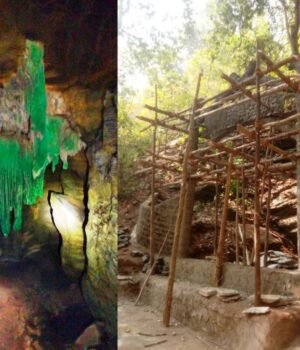Blive digital desk
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में माओवाद की जड़ें गहरी हैं, और यहां की मिट्टी में सालों से खून बहता आ रहा है। हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में विपक्ष के राज्यसभा प्रत्याशी जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने 2011 में सलवा जुडूम आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं दिया होता, तो माओवाद 2020 तक या उससे पहले ही खत्म हो चुका होता। यह बयान राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में जहां सलवा जुडूम की यादें अभी भी ताजा हैं। जस्टिस रेड्डी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सामूहिक निर्णय था, और शाह को पूरा जजमेंट पढ़ना चाहिए।
लेकिन क्या शाह का दावा सही है? आइए, इस रिपोर्ट में हम बस्तर के उस दौर की गहराई में उतरें, जहां सलवा जुडूम की शुरुआत हुई, उसकी छोटी-छोटी घटनाएं, विभिन्न पक्षों की भूमिकाएं, प्रभाव और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सच्चाई।
एक ‘शांति मार्च’ जो हिंसा की आग बना
सलवा जुडूम, जिसका गोंडी भाषा में मतलब ‘शांति मार्च’ या ‘शुद्धिकरण अभियान’ है, 2005 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों में शुरू हुआ। यह राज्य सरकार द्वारा समर्थित एक मिलिशिया था, जिसका मकसद माओवादियों (नक्सलियों) के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों को संगठित करना था। लेकिन इसकी जड़ें 1991 में महेंद्र कर्मा (पहले सीपीआई नेता, बाद में कांग्रेस विधायक) द्वारा शुरू किए गए ‘जन जागरण अभियान’ में थीं, जो नक्सलियों के खिलाफ था।
छोटी-छोटी घटनाओं ने इसे आकार दिया। 2005 में बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ स्थानीय विरोध शुरू हुआ। आदिवासी ग्रामीणों को नक्सलियों से तंग आकर छोटे-छोटे प्रदर्शन करने पड़े। उदाहरण के लिए, कुटरू और भैरमगढ़ इलाकों में नक्सलियों ने गांव वालों से जबरन लेवी वसूली और काम करवाया, जिससे गुस्सा भड़का। महेंद्र कर्मा ने इसे मौके की तरह लिया और दंतेवाड़ा, कटेकल्याण जैसे इलाकों में रैलियां कीं।
लेकिन पीछे बड़ा खेल था: राज्य सरकार ने टाटा और एस्सार जैसी कंपनियों से खनन समझौते किए थे, और नक्सली प्रभाव वाले इलाकों को ‘साफ’ करने की जरूरत थी। कहा जाता है कि इसीलिए सलवा जुडूम को हथियार और समर्थन मिला। शुरू में यह शांतिपूर्ण मार्च लगता था, लेकिन जल्दी ही यह हिंसक हो गया। जुडूम सदस्य गांवों में घुसकर घर जलाने लगे, और नक्सलियों से लड़ाई छिड़ गई।
जवानों (सुरक्षा बलों) की भूमिका: छत्तीसगढ़ पुलिस ने आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) बनाया, जिन्हें ‘कोया कमांडो’ भी कहा जाता था। वे जुडूम के साथ मिलकर नक्सलियों पर हमले करते थे, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि SPOs ने निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार किए – बलात्कार, हत्याएं और गांव जलाना। केंद्र सरकार ने भी CRPF जैसे बलों को तैनात किया, जो जुडूम को बैकअप देते थे।
माओवादियों (नक्सलियों) की भूमिका: नक्सली आदिवासियों के बीच राजनीतिक काम करते थे। भूमि अधिकार, गरीबी और शोषण पर बातें। लेकिन वे जबरदस्ती भी करते थे। जुडूम के बाद उन्होंने रणनीति बदली। छोटे ग्रुप्स में हमले, जुडूम लीडर्स को निशाना बनाना। 2008 तक वे हथियार छीनने और धमकी देने में सक्रिय हो गए। 2013 में उन्होंने झीरम घाटी हमले में छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ महेंद्र कर्मा की भी हत्या कर दी।
राजनीतिक दलों की भूमिका: कांग्रेस के महेंद्र कर्मा जुडूम के चेहरे थे, जबकि BJP की रमन सिंह सरकार ने इसे पूरा समर्थन दिया। केंद्र में UPA सरकार और तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम् ने भी SPOs की तारीफ की। लेकिन बाद में, जब हिंसा बढ़ी, कुछ नेता इसे ‘काउंटरप्रोडक्टिव’ कहने लगे। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में भी मतभेद था।
ग्रामीणों (आदिवासियों) की भूमिका: सबसे ज्यादा पीड़ित यही थे। कई को जबरन जुडूम कैंपों में ले जाया गया, जहां हालत खराब थी। कुछ नक्सलियों से डरकर जुडूम में शामिल हुए, तो कुछ जुडूम की हिंसा से नक्सलियों की तरफ चले गए। बच्चे तक SPO बनाए गए, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था।
सलवा जुडूम ने बस्तर को जंग का मैदान बना दिया। 2005 से 2011 तक हिंसा चरम पर थी। इस दौरान-
विस्थापन: करीब 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। एक लाख से ज्यादा कैंपों में या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा भाग गए। गांव खाली हो गए, आदिवासी संस्कृति बिखर गई।
मौतें और हत्याएं: कुल 800 से ज्यादा मौतें, जिनमें 300 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। SPOs में 98 मौतें (2005 में 1, 2006 में 29, 2007 में 66)। दोनों तरफ से हत्याएं जुडूम ने नक्सली समर्थकों को मारा, नक्सलियों ने जुडूम लीडर्स को।
आगजनी: जुडूम पर 600 से ज्यादा गांव जलाने का आरोप। मानवाधिकार रिपोर्ट्स में बलात्कार, बच्चे सैनिक और एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग्स का जिक्र है।
सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुड़ूम के खिलाफ याचिका
2007 में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर, हिमांशु कुमार, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं ने ध्यान दिलाया कि जुडूम राज्य-समर्थित था, जो आदिवासियों पर अत्याचार कर रहा था। जबरन विस्थापन, गांव जलाना, हत्याएं, बच्चों को SPO बनाना और मानवाधिकार उल्लंघन। उन्होंने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि राज्य नागरिकों को हथियार देकर हिंसा नहीं फैला सकता।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि पुलिस ऑपरेशनों के दौरान मार्च 2011 में 11 मार्च और 16 मार्च को बस्तर के गांवों में सैकड़ों घरों को जला दिया गया। कुल मिलाकर करीब 644 गांव खाली कराए गए और हजारों ग्रामीणों को कैंपों में रहने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ऐसे कई प्रभावित गांवों के नाम और लोगों की सूची भी प्रस्तुत की। आदिवासी परिवारों के हजारों लोग अपने घर-गांव छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए, इनमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहद खराब थी। इनमें मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा और रिहायशी सुविधाएं न के बराबर थी। उन्होंने पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी (SPO), सलवा जुडूम के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों पर बलात्कार, मारपीट, हत्या और प्रताड़ना की घटनाओं एवं सबूतों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। ताड़मेटला, तिम्मापुर जैसी जगहों पर पुलिस और SPO के उत्पीड़न व दमनशील कार्रवाईयों की केस-स्टडी बताई गईं। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। बाद में सीबीआई रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि पुलिस ने ही कई गांवों के करीब 160 से अधिक घर जलाए थे।
5 जुलाई 2011 का वह चर्चित फैसला
अंत में, 5 जुलाई 2011 को जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी और एस.एस. निज्जर की बेंच ने फैसला दिया कि जुडूम असंवैधानिक है। फैसले में कहा गया कि राज्य का नागरिकों को हथियार देकर हत्या कराना भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है। यह संविधान के मूल्यों (जीवन का अधिकार, समानता) के खिलाफ। अदालत ने जुडूम भंग करने, SPOs बंद करने और अपराधों की जांच के आदेश दिए।
अमित शाह का दावे से सहमत हों या नहीं?
शाह का दावा कि सलवा जुडूम बंद करने का फैसला न दिया गया तो 2020 तक माओवाद खत्म हो जाता, विवादास्पद है। सहमत होना मुश्किल, क्योंकि अनेक मानवाधिकार रिपोर्ट्स कहती हैं कि जुडूम ने उल्टे हिंसा बढ़ाई और नक्सलियों को मजबूत किया। 2005-2011 में 422 माओवादी मारे गए, लेकिन जुडूम की हिंसा से डरे ग्रामीण नक्सलियों की तरफ चले गए। हां, यह धारणा सही लगती है कि जुडूम ने माओवादियों को संगठित होने का मौका दिया – SPOs और सुरक्षा बलों से डरकर कई आदिवासी नक्सली बने। खनन कंपनियों के हितों ने भी इसे जटिल बनाया। आज भी बस्तर में माओवाद जारी है, जो बताता है कि सिर्फ फैसला रोकने से समस्या हल नहीं होती। अन्य पक्ष: बच्चे सैनिकों का इस्तेमाल, जो HRW रिपोर्ट में उजागर हुआ, और 2008 के बाद नक्सलियों की नई रणनीति। बस्तर के लोग आज शांति चाहते हैं, लेकिन अतीत की सच्चाई भुलाई नहीं जा सकती।
सलवा जुडूम की टाइमलाइन
📌 2005 – दंतेवाड़ा में ग्रामीणों का जनजागरण आंदोलन, बाद में सलवा जुडूम नाम मिला।
📌 2006 – राज्य सरकार का समर्थन, हजारों SPO की भर्ती, गांव खाली कराए गए।
📌 2006-08 – हिंसा, हत्याएं, आगजनी और हजारों ग्रामीण विस्थापित।
📌 2007 – मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
📌 2009-10 – बड़े मुठभेड़ और हत्याएं, राजनीतिक मतभेद गहरे।
📌 5 जुलाई 2011 – सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराया।
📌 2013 – झीरम घाटी हमले में महेंद्र कर्मा सहित कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए।
📌 2015-20 – सलवा जुडूम खत्म हुआ, पर माओवादी हिंसा जारी रही।
📌 2020 के बाद – माओवाद का दायरा सिमटा, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का अभियान जारी।