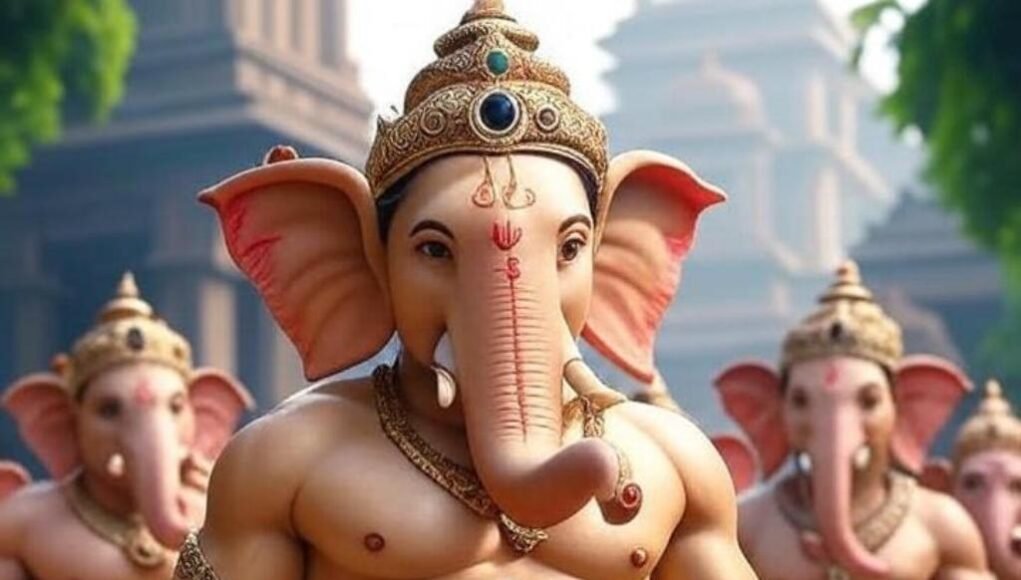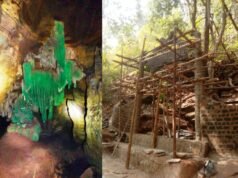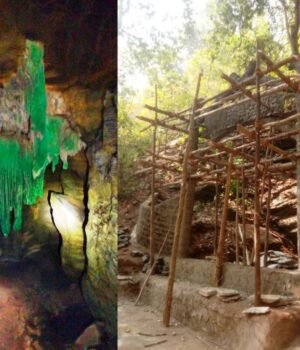रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लाखेनगर इलाके में गणेशोत्सव पंडाल में स्थापित एक प्रतिमा पर हिंदुत्ववादी संगठनों जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद (VHP) और शिवसेना के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतिमा को “AI-क्राफ्टेड डॉल-लाइक” बताते हुए मूल स्वरूप में छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके चलते पंडाल आयोजकों को प्रतिमा को परदे से ढंकना पड़ा और FIR दर्ज हुई। इसी तरह, रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के सामने अश्लील नृत्य और गीतों के खिलाफ भी बजरंग दल और अन्य हिंदू समूहों ने विरोध किया, जिसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि आयोजकों को बदलाव करने पड़े। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी साल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकारों के चेहरे काले कर दिए, क्योंकि उन्होंने गणेश प्रतिमाओं को “आपत्तिजनक” बताया। ये घटनाएं गणेश की प्रतिमाओं के “मूल” स्वरूप को लेकर उठने वाले विवादों को दर्शाती हैं, जहां पारंपरिक छवि (हाथी का सिर, लंबा उदर, एक दंत, मूषक वाहन) से विचलन को अस्वीकार किया जाता है।
गणेश की लोकायत धारणा: विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता तक
हिंदू पौराणिक कथाओं और लोकायत परंपराओं में गणेश (जिन्हें गणपति, विनायक या गणेश्वर भी कहा जाता है) की छवि शुरुआती काल में मुख्य रूप से “विघ्न पैदा करने वाले” देवता के रूप में थी। वे “गणों” (भूत-प्रेत, यक्ष या दैत्य जैसे अदृश्य प्राणियों के समूह) के अध्यक्ष या नेता माने जाते थे। इन गणों को अक्सर विघ्न (बाधाएं) पैदा करने वाला माना जाता था, और गणेश को उनका नियंत्रक। इसलिए, उनकी पूजा अक्सर भय या विघ्नों से बचाव के लिए की जाती थी, न कि केवल शुभता के लिए। समय के साथ, यह धारणा विकसित हुई और गणेश को “विघ्नहर्ता” (बाधाओं का नाशक) के रूप में पूजा जाने लगा, खासकर किसी नए कार्य की शुरुआत में। उदाहरण के लिए, विघ्नेश्वर नाम का अर्थ है “विघ्नों का स्वामी”, जो बाधाएं डालने और हटाने दोनों को दर्शाता है। यह लोकायत विश्वास प्राचीन वैदिक या प्राक्-आर्य परंपराओं से जुड़ा हो सकता है, जहां गणेश जैसे देवताओं को प्रकृति की अराजक शक्तियों का प्रतिनिधि माना जाता था।
इतिहासकारों और विद्वानों की राय
इतिहासकार और पौराणिक विद्वान गणेश की उत्पत्ति को मुख्य रूप से गैर-वैदिक या लोक परंपराओं से जोड़ते हैं, जो बाद में मुख्यधारा हिंदू धर्म में समाहित हुई।
- प्राचीन उत्पत्ति और विकास: गणेश का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में नहीं मिलता, लेकिन महाभारत और पुराणों (जैसे स्कंद पुराण, मुद्गल पुराण) में है। इतिहासकारों के अनुसार, गणेश की अवधारणा 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास ठोस रूप लेती है, जब उनकी मूर्तियां भारत में प्रचलित हुईं। विद्वान जैसे रॉबर्ट ब्राउन (Ganesa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings) गणेश को “गणों का पति” मानते हैं, जहां गण प्राचीन जनजातीय या लोक देवताओं के समूह थे, जो विघ्न पैदा करते थे। पूजा भय से शुरू हुई, क्योंकि उन्हें प्रसन्न न करने पर वे बाधाएं डालते थे। कुछ इतिहासकार (जैसे ए.के. नारायण) इसे द्रविड़ या प्राक्-आर्य परंपराओं से जोड़ते हैं, जहां हाथी जैसे प्रतीक शक्ति और विघ्नों का प्रतिनिधित्व करते थे।
- विघ्नकर्ता की भूमिका: पुराणों में गणेश को कभी-कभी विघ्न पैदा करने वाला दिखाया गया है, लेकिन बाद में शिव-पार्वती की कथाओं से जुड़कर वे विघ्नहर्ता बने। इतिहासकारों का मानना है कि यह परिवर्तन 8वीं-10वीं शताब्दी में हुआ, जब गणेश को बुद्धि, कला और शुभता का देवता बनाया गया।
- समाजशास्त्रीय दृष्टि: विद्वान जैसे अनीता रैना थापन (Understanding Ganapati) गणेश की पूजा को सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बताते हैं, जहां विघ्नों का भय लोगों को अनुशासित रखता था। यह धारणा आदि काल में मजबूत थी, लेकिन मध्यकाल में लोकप्रिय उत्सवों (जैसे गणेश चतुर्थी) ने इसे सकारात्मक बना दिया।
मूल स्वरूप, आकृति और शारीरिक संरचना
गणेश की आधुनिक छवि (हाथी का सिर, मानव शरीर, लंबा उदर, एक दंत, मूषक वाहन) बाद के विकास का परिणाम है। मूल स्वरूप अधिक सरल और प्रतीकात्मक था:
- मूल स्वरूप: प्राचीन मूर्तियों (5वीं-6वीं शताब्दी) में गणेश को हाथी के सिर वाला, लेकिन बिना पोटबेली या टूटे दंत के दिखाया गया है। वे “विनायक” के रूप में गणों के नेता थे, शायद बिना किसी विशेष वाहन के। आकृति मुख्य रूप से मिश्रित (हाइब्रिड) थी: हाथी सिर प्राकृतिक शक्ति और बुद्धि का प्रतीक, जबकि शरीर मानव जैसा। कुछ प्राचीन चित्रणों में वे सर्प से बंधे दिखते हैं, जो ऊर्जा का प्रतीक है।
- बाद में विकसित धारणाएं:
- एक दंत (टूटा हुआ दांत): यह 8वीं शताब्दी के बाद प्रमुख हुआ, जो भावनाओं पर बुद्धि की विजय का प्रतीक है (दाहिना दांत बुद्धि, बायां भावना)।
- लंबोदर (पोटबेली): भौतिक समृद्धि और ब्रह्मांड को समाहित करने का प्रतीक, 10वीं शताब्दी के बाद प्रचलित हुआ।
- मूषक की सवारी: यह भी बाद का विकास है (मुद्गल पुराण आदि में उल्लेख है), जो छोटी बाधाओं पर विजय का प्रतीक है। मूल में कोई वाहन नहीं था।
कुल मिलाकर, गणेश की धारणा समय के साथ लोक से पौराणिक और फिर उत्सव के रूप में बदली। 2025 की घटनाएं इसी “मूल” vs “आधुनिक” विवाद को उजागर करती हैं, जहां परंपरावादी समूह पारंपरिक छवि को संरक्षित रखना चाहते हैं।